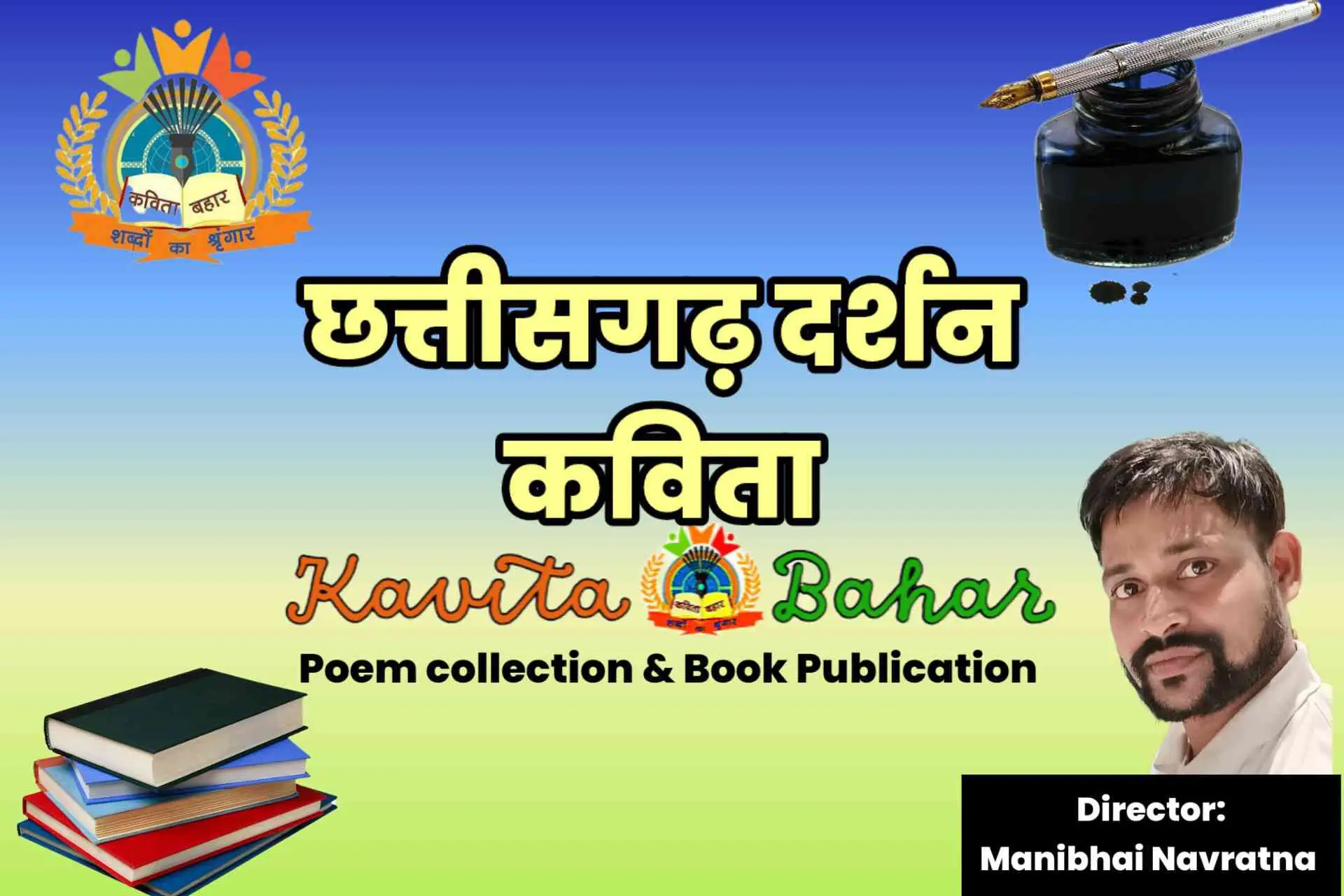मनीभाई नवरत्न की कविता “धूल का पांडुलिपि” एक लेखक की अनकही कहानी बयान करती है, जो समाज की सच्चाई को शब्दों में पिरोती है। पढ़ें यह भावनात्मक और विचारोत्तेजक रचना।
कविता का उद्देश्य
“धूल का पांडुलिपि” कविता का उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता, उपेक्षा और मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी को उजागर करना है। यह एक लेखक के सपनों और उसकी रचना की अनसुनी कहानी के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयों को दर्शाती है। कविता यह प्रश्न उठाती है कि क्या साहित्य और कला की सच्चाई को व्यावसायिकता और बाजार की माँगों के आगे झुकना पड़ता है। यह पाठकों को गहरे चिंतन और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उन अनकही कहानियों की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो धूल में दबकर रह जाती हैं।
धूल का पांडुलिपि
पुराने शहर के
एक संकरे मोहल्ले में,
एक कमरे की पीली दीवारों के बीच,
एक लेखक बैठा था।
उसकी मेज़ पर रखी थी
एक मोटी-सी पांडुलिपि—
बिना जिल्द की,
बिना शीर्षक की।
उसने इसे महीनों में लिखा था—
शब्दों में चूल्हों का धुआँ,
वाक्यों में आधी रात का सन्नाटा,
और पन्नों के किनारों पर
आँसुओं की हल्की-सी नमी।
लेखक को लगता था,
“जब ये किताब बाज़ार में जाएगी,
लोग पढ़कर रो पड़ेंगे,
शायद कुछ बदल जाएगा।”
वह पांडुलिपि लेकर
बड़े-से बाज़ार पहुँचा।
वहाँ की दुकानों में
रंगीन जिल्द वाली किताबें सजी थीं—
“सात दिन में करोड़पति”,
“मुस्कान से जीतिए दुनिया”,
और चमकीली तस्वीरों से भरी
कॉफ़ी टेबल बुक्स।
एक प्रकाशक ने पन्ने पलटे,
भौंहें सिकोड़कर कहा—
“शब्द भारी हैं…
हमारे ग्राहक हल्का पढ़ना पसंद करते हैं।”
दूसरे ने मुस्कुराकर कहा—
“ये तो बहुत उदास है,
कॉफ़ी के साथ ठीक नहीं लगेगा।”
लेखक चुपचाप लौट आया।
उसने पांडुलिपि को
कमरे के एक कोने में रख दिया।
दिन बीतते गए,
धूल जमा होती गई।
मोहल्ले के बाहर,
वही कहानियाँ अब भी जी रही थीं—
भूख अभी भी थालियों में परोसी जा रही थी,
आसमान अब भी सूखा था,
और चूल्हों का धुआँ
अब भी आँखों को जलाता था।
बस फर्क इतना था—
किताब धूल में दबी रही,
और भूख…
वो हर जगह,
बिना पन्नों, बिना जिल्द,
मुफ़्त में बँटती रही।
मनीभाई नवरत्न
भौंरादादर, बसना
महासमुंद